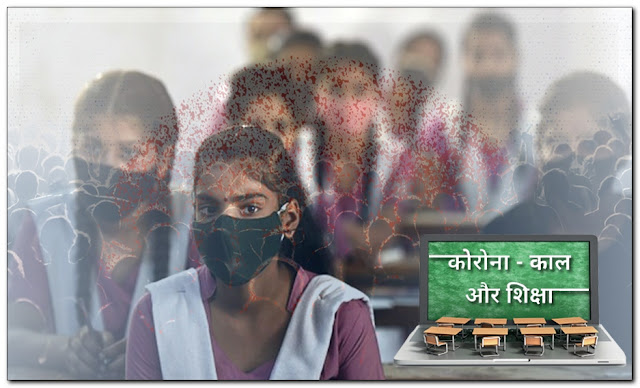जब जनवरी-फ़रवरी 2021 में दूसरी लहर की चेतावनी जारी की जा रही थी, तभी अनेक राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारियाँ हो रही थी! पता नहीं कैसे? फिर दूसरी लहर ने कहर ढाया। महज़ कुछ दिनों तक शिक्षा कार्य जारी रखने के बाद बंद करना पड़ा। फिर जब जुलाई-अगस्त 2021 में तीसरी लहर को लेकर चेतावनियाँ घूम रही थीं, फिर से स्कूल खोलने की तैयारियाँ शुरू हुईं! पता नहीं कैसे? कई लोग पूछते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलता है? और इसका कोई सटीक और ठोस जवाब नहीं है।
न जाने कितना कितना
और कैसा कैसा बोला और कहा जा रहा था कुछ सालों पहले। इन दो सालों में हर जगह अब लोग
ऑफलाइन की महत्ता को लेकर बातें कर रहे हैं। वो सारा प्रचार-प्रसार भूगर्भ गटरों में
बह गया है। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर हमारी व्यवस्थाएँ कितनी फिसड्डी हैं यह बात इस समय
सभी को समझ आ ही गई होगी। ख़ैर, यहाँ बात हमें दूसरी चीज़ की करनी है, तो उसी तरफ़ आगे बढ़ते हैं।
पढ़े नहीं, लेकिन पास हो गए!!! इस समय चक्र से बाहर
अनेक छात्र निकलना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते होंगे, लेकिन जो चाहते हैं
उनकी तो बात हो ही सकती है न। अगर आपने मूल पढ़ाई ही नहीं कि और आप अगली क्लास में
आ गए, तो यह महामारी की आपातकालीन स्थिति की मजबूरी थी। कोरोना वायरस तो शायद एक मौसमी
बीमारी भी बन कर रह जाए, ऐसे में शिक्षा से यूँ वंचित तो रहा नहीं जा सकता। ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन की
सुविधा बहुधा समाज के पास नहीं है। उनको भी वंचित नहीं रखा जा सकता। ऑफलाइन शिक्षा
के फ़ायदे और ऑनलाइन शिक्षा के नुक़सान समाज देख रहा है।
कोरोना महामारी के
दौरान बच्चों के लिए स्कूलों में शिक्षाकार्य शुरू किया जाए या नहीं, अब भी सबसे बड़ा सवाल
यही घूम रहा है। कमाल यह कि इसके पीछे जो मुख्य वजहें हैं उसकी बात नहीं हो रही। ऑनलाइन
एजुकेशन में फिसड्डी साबित होने के बाद ऑफलाइन एजुकेशन ‘मजबूरी’ बन गया है यह तथ्य
देखा नहीं जा रहा। उपरांत देश के बहुधा लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने के
संसाधन ही मौजूद नहीं हैं, इस स्थिति में महीनों से शिक्षा से वंचित उन बच्चों का वर्तमान और भविष्य भी एक
बड़ा मुद्दा है। साथ ही जिनके पास संसाधन हैं वहाँ पर भी स्कूल, स्कूल के शिक्षक, स्कूल का प्रशासन, बच्चे, अभिभावक, सभी ने एक साथ मिलकर
ऑनलाइन एजुकेशन को जिस तरह फिसड्डी साबित किया, वह भी बड़ी वजह मानी जा सकती है।
जोखिम यह है कि शायद
एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह जाए। और यह अपने आप में कई सारे ख़तरों का सूचक है।
ऑनलाइन तरीक़ों को अब तक अग्रता देने की सनक धारण करने वाला समुदाय अब ऑफलाइन तरीक़ों की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा का महत्व, मानसिकता, बच्चों पर प्रभाव समेत दूसरे तमाम अनगिनत फ़ायदों से अब लोग परिचित होने लगे हैं।
इन सब स्थितियों के
बीच भी अभिभावकों को एक ही चिंता है। और वो चिंता है अपने बच्चों के स्वास्थ्य की, उनकी ज़िंदगी की। जो
बच्चे 10वीं, 12वीं कक्षा में या उससे आगे अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए स्थिति और विकट है।
Corona & Testing Kits: दुनिया अपने नागरिकों का टेस्टिंग कर रही थी... हम टेस्टिंग किट के टेस्ट में ही अटके हुए थे!
सर्वे में आप केवल
एक ही सवाल रखते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन? लेकिन ऑफलाइन क्यों पसंद करने को मजबूर हैं यह सर्वे थोड़ी न दिखाएगा। आज भी कई
अभिभावक कहते हैं कि यदि स्कूल वाले बढ़िया तरीक़े से ऑनलाइन एजुकेशन चलाते हैं तो हम
अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे।
कोरोना की दूसरी लहर
के बाद विशेषत: छोटे बच्चों को लेकर शिक्षा का कार्य ऑफलाइन शुरू किया जाए या वह कार्य फ़िलहाल ऑनलाइन ही जारी रखा जाए, इस विषय को लेकर काफ़ी माथापच्ची हुई। अलग अलग रिपोर्टें, अलग अलग सर्वे को
आधार बनाकर वातावरण ऐसा बना दिया गया कि ज़्यादातर अभिभावक ऑफलाइन शिक्षा कार्य शुरू
करने के पक्ष में हैं।
विशेषक्षों के हवाले
से रिपोर्टें आईं, समितियों ने अपनी रिपोर्टें दीं, अलग अलग सर्वे को आगे किया गया। सब में बड़ी बात यही रखी गई कि ज़्यादातर विशेषज्ञ
और ज़्यादातर अभिभावक ऑफलाइन शिक्षा कार्य शुरू करने के पक्ष में हैं। कभी कुछ सर्वे
छपे, कभी कुछ और। सर्वे में प्रतिशत भी लिखे गए। लिख दिया गया कि इतने प्रतिशत अभिभावक
चाहते हैं कि ऑफलाइन शिक्षा कार्य शुरू किया जाना चाहिए और इतने प्रतिशत अभिभावक नहीं
चाहते, वगैरह वगैरह चीज़ें लिखी-कही जाने लगी।
शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए इस महामारी की
स्थिति में, यह अभिभावकों की अपनी चिंता है। स्कूल और स्कूल के प्रशासन से उन्हें जितने सुरक्षा
मानक हैं, उन मानकों के पालन की उम्मीद है, क्योंकि अभिभावक उस
राम राज्य को देख चुके हैं दूसरी लहर के दौरान। सुरक्षा मानकों का सरेआम उल्लंघन नेता, सेलेब्स से लेकर लोगों
तक ने घड़ल्ले से किया है। सुरक्षा मानक ढेरों होते हैं, लेकिन उन मानकों का पालन नहीं
होता। अभिभावकों को उम्मीद है कि कम से कम बच्चों के लिए स्कूलों के भीतर वो सारी कमियाँ
न रहे, जो बाहर दिखाई दे रही हैं। और उस चिंता की तरफ़ कोई समिति नहीं देख रही, कोई विशेषज्ञ उन मनों
को टटोल नहीं रहा।
किसी नेता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री
को लेकर जिस प्रकार के सर्वे छपते रहते हैं, बिलकुल इसी तरह शिक्षा कार्य को लेकर सर्वे छपने लगे। इन सर्वे को लेकर धड़ल्ले
से लिखा जा सकता है कि 75 फ़ीसदी से ज़्यादा अभिभावकों के पास कोई सर्वे वाला नहीं गया
होगा, ना किसी ने उनसे उनकी राय पूछी होगी। शिक्षा कार्य शुरू किया जाए या नहीं, इसका सर्वे अभिभावकों
के घरों में हो गया यह अभिभावकों को ही नहीं पता!!! किसी ने यह नहीं लिखा कि अभिभावक
यह भी चाहते हैं कि यदि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बढ़िया तरीक़े से हो तो अब भी बहुत सारे
अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। यह बात किसी सर्वे ने, किसी समिति ने क्यों
नहीं लिखी, इसे कौन सोचेगा भला?
12 अगस्त 2021 के दिन
दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट की है कि स्कूल खुलते ही बच्चे कोरोना से संक्रमित होने लगे
हैं। अख़बार ने लिखा है कि बैंग्लुरु में एक सप्ताह के भीतर ही 300 से ज़्यादा बच्चे
कोरोना से संक्रमित हो गए। दिव्य भास्कर ने दावा किया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों
में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के मामले मिल रहे हैं।
कुछ राज्यों के नाम
लिखे हैं तो ऐसा न माने कि उन राज्यों में ही ऐसी स्थिति होगी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों
में स्कूल खुलने से पहले ही बच्चों में कोरोना संक्रमण मिलने के मामले सामने आ चुके
हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में दूसरी लहर के बाद (यूँ कहे कि दूसरी लहर के बीच) अगस्त
2021 में स्कूल खुले और फिर उसी महीने में कुछ दिनों तक स्कूल बंद कर दिए थे। पंजाब
अपने स्कूलों में आरटी पीसीआर टेस्ट कराने को मजबूर हो चला है।
31 अगस्त 2021 के दिन
एनडीटीवी की रिपोर्ट थी, जिसके मुताबिक़ स्कूल खोलने वाले ज़्यादातर राज्यों में बच्चों में कोरोना संक्रमण
के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट की माने तो ऐसे राज्यों में पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उतराखंड और गुजरात
शामिल थे। रिपोर्ट के भीतर अलग अलग राज्यों में बच्चों के संक्रमण में वृद्धि का प्रतिशत
दर्ज किया गया था।
यूँ तो एक तरफ़ कोरोना
की तीसरी लहर को लेकर बातें जम कर हो रही हैं। इन बातों और आशंकाओं के बीच स्कूलें
भी जमकर खोली जा रही हैं। जनवरी-फ़रवरी 2021 का दौर याद आ रहा है, जब दूसरी लहर की आशंका
जताई जा रही थी और इस बीच स्कूलें खोली जा रही थी!!! इस रिश्ते को समझना फ़िलहाल तो
नामुमकिन है।
हमें एक बात बिलकुल समझनी होगी कि हम तीसरी
लहर की बात कर रहे हैं, किंतु दूसरी लहर अब भी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है कि दो-तीन राज्यों में ही देश
के कुल मामलों के 65 से 75 फीसदी मामले मिल रहे हैं। किंतु रोज़ाना आँकड़ा अब भी हज़ारों
में हैं। मार्च 2020 में देश भर में रोज़ाना जितने संक्रमित मिलते थे, आज रोज़ाना उतने लोग
कोरोना की वजह से मारे जा रहे हैं!!! कोरोना की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है। कई राज्यों
में अब भी तरह तरह के बैन जारी है। केरल और महाराष्ट्र अब भी झूज रहे हैं।
जिस राज्य में सबसे
दुखदायी नज़ारा देखने को मिला था वहाँ भी स्कूल खुल गए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे
हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में माँ गंगा की गोद में जिस तरह से
सैकड़ों लाशें तैरती दिखी, यह कोरोना की त्रासदी का वह मंज़र था, जिसे कभी भूलाया नहीं जा सकता। यहाँ भी गाँव-गाँव
शहर-शहर कतारों में जलती चिताओं की तसवीरें देखने को मिली थी। यही सच्ची विभीषिका थी।
ऐसे राज्य में स्कूल खुल गए तो फिर बाकी जगहों पर खुलने ही थे।
यूँ तो ज़्यादातर राज्यों ने तय किया है कि
पहले सीनियर स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, फिर जूनियर को। हमारे
यहाँ गुजरात समेत देश के कई राज्यों ने '50-50 वाला फॉर्मूला’ अपनाया है। यानी, एक क्लास में 50 प्रतिशत
बच्चों को ही एक दिन में बुलाया जाएगा। पहली नज़र में यह अच्छा लगता है। लेकिन इस फॉर्मूला
को क़रीब से और ज़मीनी स्तर पर देखे तो यह फॉर्मूला ‘प्रशासन की बेवकूफ़ी’ का सिंबल जैसा भी
लगता है।
फिर एक मान्यता यह भी उभरी थी कि सभी को होता है, लेकिन बच्चे सुरक्षित
हैं। इसके पीछे कुछ तर्क भी दिए जाते थे। फिर कोरोना वायरस ने बच्चों को भी संक्रमित
करना शुरू किया। मान्यता फिर एक बार सहुलियत के हिसाब से बदल गई। कहा जाने लगा कि कम
बच्चे संक्रमित हुए हैं। लेकिन पुरानी मान्यता को मार कर यह ज़रूर मान लिया कि बच्चे
भी संक्रमित होते हैं।
फिर कुछ देशों में ज़्यादा बच्चे संक्रमित होने लगे तो एक और
तर्क आया कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक शक्ति होने की वजह से कुछ नहीं होगा। तभी वायरस
के जानकारों ने चेता दिया कि बच्चों को कुछ नहीं होगा वाले तर्क से संतुष्ट मत रहें, क्योंकि वे वायरस
के वाहक हो सकते हैं और दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता धारण किए हुए होते हैं।
सोचिए, एक साल में कितनी सारी धारणाओं, मान्यताओं को विशेषज्ञों ने बदल लिया।
वायरस के जानकार तो पहले से स्पष्ट थे और
संयमित भी, उधर विशेषज्ञ सहुलियत के मुताबिक़ ख़ुद को और ख़ुद के मतों व बयानों को बदलते रहे।
अगस्त 2021 के मध्य
काल में नीति आयोग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कुछ सलाह दी थी। आयोग ने मंत्रालय
को सूचित किया कि स्थानीय स्तर पर संक्रमण के हालात को देखते हुए स्कूल खोलने का फ़ैसला
लिया जा सकता है। हालाँकि आयोग ने एक सलाह यह भी दि कि कम से कम 70 फ़ीसदी शिक्षकों
और स्टाफ़ का टीकाकरण हुआ हो तब आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं है। आयोग ने जनसंख्या और
संक्रमण के गाणितीय आधार पर कुछ आँकड़े भी दिए। आयोग ने आगे शिक्षा मंत्रालय को सूचित
किया कि स्टाफ़ का टीकाकरण, इलाके में संक्रमण का दर, इन दोनों के तुलना में एक रेशियो बनाकर उस हिसाब से ही उतनी ही तादाद में स्टूडेंट
को स्कूल बुलाया जाए। आयोग ने उस स्टाफ़ का साप्ताहिक आरटी पीसीआर टेस्ट कराने को कहा, जिनका टीकाकरण हो
नहीं पाया है।
हालाँकि ज़्यादातर राज्यों
में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक ही आदेश। 50-50 वाला फॉर्मूला। आयोग ने साथ ही दूसरे तमाम
सुरक्षा मानकों पर भी जोर दिया।
कोरोना के कारण लंबे
समय से बंद पड़े स्कूलों को लेकर एक संसदीय समिति ने भी अपनी चिंता ज़ाहिर की और कहा
कि स्कूलों का खोला जाना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च, यानी आईसीएमआर के प्रमुख बलराम भार्गव भी एहतियात के साथ प्राइमरी स्कूल और फिर सेकेंडरी
स्कूल खोले जाने का सुझाव दे चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28
अगस्त 2021 के दिन कहा था कि अब पेरेंट्स भी आकर कहते हैं कि जल्दी जल्दी स्कूल खोलो।
आईएमए के अध्यक्ष डॉ. जेए जयलाल ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की संभावना
को मद्देनज़र रखते हुए इस समय जोखिम बहुत नगण्य है, यह सही समय है जब सरकार को आगे आकर एक परिकलित जोखिम लेना चाहिए
और उचित तरीक़े से स्कूल खोलने चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली
में 70 फ़ीसदी अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल खोले जाए।
ऑनलाइन एजुकेशन में
हर जगह गणित, विज्ञान जैसे विषयों में ढेरों दिक्कतें पेश आ रही हैं। बच्चों में जो आधारभूत
ज्ञान होना चाहिए उसकी कमी भी सामने आ रही है। मानसिक विकास वाला फ़ायदा तो बच्चों को
मिल ही नहीं पा रहा।
उधर 7 अगस्त 2021 के
दिन कोविड कोर कमेटी के सदस्य डॉ. पार्थिव मेहता ने चेताते हुए कहा था कि यह समय वायरल
इंफेक्शन का भी है, क्रोस वायरल इंफेक्शन तेज़ी से फैल रहा है, छोटे बच्चे कोरोना वायरस के करियर बन सकते हैं, कुछ संक्रमित हो सकते हैं, कुछ दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स, विशेषज्ञ, शिक्षक, समुदाय ऐसे भी हैं, जो छोटे बच्चों के
लिए स्कूल खोलने को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति रखने के पक्ष में है।
एक बात तो अब लोग समझ
ही चुके हैं कि ऑफलाइन एजुकेशन ही बेहतर है, ऑनलाइन एजुकेशन वाला तरीक़ा तो आपातकालीन स्थिति के लिए था। बहुत सीधी बात है कि
लंबे समय तक शिक्षा कार्य बंद रखना बच्चों के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत सारे ख़तरे ले आएगा। घर की चार दीवारी के भीतर पढ़ने से किसी बच्चे को वह सारे फ़ायदे प्राप्त नहीं
हो सकते, जो स्कूल जाकर पढ़ने से मिलते हैं। यह फ़ायदे अनेका अनेक प्रकार के होते हैं।
सर्वे, समितियाँ वगैरह जैसी
बातें छोड़ दें और ज़मीनी हक़ीक़त के आधार पर सैकड़ों लोगों के साथ बातें करके अनेक मीडिया
रिपोर्टें आई हैं उन मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करें तो वह विश्लेषण कुछ तथ्यों की तरफ़ ले जाता
है। पहला यह कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादातर तो विफल रहा है और इसके पीछे सभी का हाथ है, किसी एक का नहीं।
दूसरा यह कि अगर बेहतर ढंग से ऑनलाइन एजुकेशन मिले तो आज भी कम उम्र के बच्चों को स्कूल
नहीं भेजने का इरादा रखने वाले अभिभावकों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा यह कि ज़्यादातर अभिभावकों को चिंता यह है कि स्कूल और स्कूल का प्रशासन क्या उन तमाम मानकों
का सही ढंग से पालन कर पाएँगे? और सबसे बड़ा तथ्य यह कि शिक्षा की ज़रूरत और उस ज़रूरत पूरी करने के तरीक़े महामारी
के दौर में बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ साथ स्कूल, शिक्षकों और स्कूल
के प्रशासन के सामने कई सारी दिक्कतें पेश कर रहे हैं।
50-50 वाले फॉर्मूला
पर भी मत अलग अलग ही रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सीधा सीधा मानना है कि क्लास
में जो संख्या है उसके अनुपात को देखते हुए छात्रों को बुलाना चाहिए। छोटे बच्चे एक
साथ 50 या उससे ज़्यादा तादाद में उपस्थित रहेंगे तो किसी सुरक्षा मानक का पालन नहीं
हो पाएगा।
उपरांत अभिभावकों से
संमति पत्र लिखाने की प्रथा के साथ साथ अभिभावकों को स्कूल का स्टाफ़, स्कूल की तैयारियाँ, आदि की जानकारी देना भी ज़रूरी माना गया है। लेकिन इस पर ना स्कूल वाले गंभीर हैं, ना सरकारी प्रशासन
वाले। स्कूल के स्टाफ़ का टीकाकरण, इसमें भी कितने प्रतिशत का टीकाकरण होना ज़रूरी है इस मत में अंतर तो है, साथ ही कितनों का
टीकाकरण हुआ है उसकी जानकारी अभिभावकों को देने की बात पर भी मतभेद हैं।
कुल मिलाकर आप किसी ठोस तरीक़े से यह नहीं
कह सकते कि कितने फ़ीसदी अभिभावक क्या चाहते हैं। इसका प्रतिशत निकालना मुमकिन ही नहीं
है। साथ ही ग़ैरज़रूरी भी है। प्रतिशत या सर्वे जैसी चीज़ों में समितियाँ व्यस्त रहे
उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जिन तरीक़ों को लागू करना है उसमें बेहतरी और सुरक्षा के
स्थायी प्रबंध किए जाए। ढेर सारी ज़मीनी रिपोर्टों को देखकर एक पत्रकार मित्र से पूछ
लिया कि क्या इसका मतलब यह माना जाए कि दूसरी लहर से पहले ऑनलाइन एजुकेशन एक मजबूरी
था और अब दूसरी लहर के बाद ये ऑफलाइन एजुकेशन एक मजबूरी है? जवाब मिला कि पक्का
तो कुछ नहीं कह सकते, शायद कुछ हद तक बात सही भी हो। क्योंकि दूसरी लहर का जो कहर था, उस कहर ने बहुत कुछ
बदल दिया है। जिन परिवारों ने या जिनके स्वजनों ने वह त्रासदी झेली उनके लिए तो कौन
सा तरीक़ा पकड़े यह तय कर पाना वाक़ई कठीन समय है। उधर जिनके पास पहले वाले तरीक़े के
लिए संसाधन ही नहीं है, उनके लिए रास्ता चुनने का विकल्प ही कहाँ है?
दूसरी तरफ़ वह दौर भी मुँह फाड़े खड़ा है जब
देश में नेता, सेलेब्स से लेकर आम जनता तक ने घड़ल्ले से कोरोना से संबंधित नियमों को तोड़ा
और बेफ़िक्र व बेपरवाह घूमते रहे। आम जनता में वे लोग भी होंगे, जिनके बच्चे स्कूलों
में जाने को तैयार हो रहे हैं या जाने लगे हैं। तो फिर एक सोच यह भी मन में आती है
कि ऐसे अभिभावक, जिन्होंने स्वयं उन नियमों को ताक पर रखा, वे अपने बच्चों को
किस तरह समझाएँगे, किस तरीक़े से उन्हें तैयार करेंगे? उनके अपने माता-पिता, उनका अपना परिवार
नियमों को तोड़ कर भीड़ में जाता रहा, हिल स्टेशनों पर घूमता रहा। ऐसे परिवारों
के बच्चे अपने अभिभावकों से “जागरूकता की शिक्षा” कैसे प्राप्त करेंगे?
शिक्षा कार्य शुरू करना चाहिए या नहीं इसे
लेकर जितनी भी चर्चा हुई, प्रमुख बात रही कोरोना वायरस को लेकर स्कूलों में सुरक्षा मानकों के पालन की।
जब कोरोना वायरस नहीं था तब भी देश के ज़्यादातर स्कूलों में क्या हालात रहे थे वह सोचना
भी ज़रूरी है। ज़्यादातर स्कूलों के जो हालात है, यह सवाल उठना लाज़मी
है कि क्या वहाँ उन तमाम सुरक्षा मानकों का पालन हो पाएगा, जो कोरोना वायरस की
महामारी के दौर में ज़रूरी है?
स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए इसे
लेकर बहुत माथापच्ची होती रही। अभिभावकों, शिक्षकों, बच्चों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, समाजशास्त्री... अलग
अलग प्रकार के कई लोगों ने अपना अपना माथा खपाया। फिर तो सर्वे आने लगे। सर्वे की ख़ास
बात यह रही कि अभिभावकों की इच्छा का प्रतिशत भी आ गया, किंतु बहुत ही ज़्यादा अभिभावकों को पता ही नहीं चल पाया कि उनकी इच्छा का प्रतिशत निकाला जा रहा है!!! करोडों
अभिभावकों में से शायद 75 फ़ीसदी से भी ज़्यादा अभिभावकों के पास कोई सर्वे वाला गया
ही नहीं होगा। फिर भी अभिभावकों की इच्छा का प्रतिशत निकल आया!!!
(इनसाइड इंडिया, एम वाला)